यह है दुनियां का सबसे बड़ा रहस्य ,क्या है जीवन, क्या है प्राण, कैस होती है ईश्वर की प्राप्ति
यह है दुनियां का सबसे बड़ा रहस्य ,क्या है जीवन, क्या है प्राण, कैस होती है ईश्वर की प्राप्ति
जीवन का आनन्द केवल वोहि व्यक्ति ले सकता है जो समय की महत्ता को समझेगा, इस कार्य को इस उदाहरण से समझने की कोशिश किजिएगा।
अगर मानलों आपके 100 रूपये कहीं गिर जाते हैं और आप उनकों ढुडने की कोशिश करते हो और न मिलने पर आप दुःख विलिन हो जाते हो आप अपना कुछ समय उसी दुःख के कारण खराब करते हों तो क्या आपके कीमती सयम की कीमत उस 100 रूपये से भी कम हैं बस यहां इतना ही समझना होगा कि - खोया हुआ धन वापस आसकता है परन्तु खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता

प्राण साक्षात् ब्रम्हा से अथवा प्रकृति रूपी माया से उत्पन्न है। प्राण गत्यात्मक है। इस प्राण की गत्यात्मकता सदा गतिक वायु में पाई जाती है। शरीरगत स्थानभेद से एक ही वायु प्राण, अपान आदि नामों से व्यह्रत होता है। प्राण षक्ति एक है। इसी प्राण को स्थान व कार्याे के भेद से विविध नामों से जाना जाता है। देह मंे मुख्य रूप से पाँच प्राण तथा पाँच उपप्राण है।

1. प्राण- शरीर में कंठ से लेकर ह्रदय जो वायु कार्य करता है, उसे ‘प्राण’ कहा जाता है।
कार्य- यह प्राण नासिक मार्ग, कंठ, स्वर तंत्र, वाक्-इन्द्रिय, अन्न-नलिका, शवसन तंत्र, फेफड़ों को क्रियाशीलता तथा शक्ति प्रदान करता है।
2. अपान- नाभि से नीचे से लेकर पैर के अंगुश्ठ पर्यन्त जो प्राण कार्यशील रहता है, उसे ‘अपान प्राण’ कहते हैं।
कार्य- शरीर में संगृहीत हुए समस्त प्रकार के विजातीय तत्वों अर्थात मल व मूत्र आदि को बहार कर देह शुद्धि का कार्य ‘अपान’ प्राण करता है।
3. उदान - कंठ से ऊपर शरीर से लेकर सिर पर्यन्त देह में अवस्थित प्राण को ‘उदान’ कहते हैं।
कार्य-कंठ के ऊपर शरीर के समस्त अगों नेत्र, श्रोत्र, नासिक व सम्पुर्ण मुख मण्डल को ऊर्जा व आभा प्रदान करता है।
4. समान - ह्रदय से नीचे से लेकर नाभि पर्यन्त शरीर में क्रियाशील प्राण को ‘समान’ कहते है।
कार्य- यकृत, आंत्र, प्लीहा व अन्याशय (च्ंदबतमंे) सहित सम्पुर्ण पाचन तंत्र की आन्तरिक कार्य प्रणाली को नियन्ति करता है।
5. व्यान- यह जीवनी प्राण शक्ति पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर की समस्त गतिविधियों को नियमित तथा नियन्त्रित करता है।
ये है छींक आने का कारण

हम क्यांे छीकते हैं, क्यों जमाई लेते हैं और क्यांे खुजलाते हैं जानों ये उपप्राण क्या होता हैं पँाचों प्राणों के अतिरिक्त शरीर में ‘देवदत्त’,‘नाग’,‘कृकल’, ‘कूर्म’, ‘धनंजय’ नामक पाँच उपप्राण होते हैं जो क्रमश है छीकना, पलक छपकना, जमाई लेना, खुजलाना तथा हिचकी लेना आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं।
शरीर में आत्मा किस रूप मे रहती है। आखिरकार क्या होता है। पंचकोश

मनुष्य की आत्मा पाँच कोशो के साथ संयुक्त है। जिन्हें पंच शरीर भी कहते हैं ये पाँच कोश निम्नानुसार होते है।
1. अन्नमय कोश- यह पंचभौतिक स्थूल शरीर का पहला भाग है। अन्नमय कोश त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त पृथ्वी तत्व से सम्बन्धित है। आहार-विहार की शुचिता, आसन-सिद्ध होती है।
2. प्राणमय कोश- शरीर का दुसरा भाग प्राणमय कोश है। शरीर और मन के मध्य में प्राण माध्य है। ज्ञान कर्म के सम्पादन का समस्त कार्य प्राण से बना प्राणमय कोश ही करता है। श्वासोच्छवास के रूप में भीतर-बाहर जाने-आने वाला प्राण स्थान तथा कार्य के भेद से 10 प्रकार का माना जाता है। जैसे-व्यान, उदान, प्राण, समान, अपान मुख्य प्राण हैं तथा धनंजय, नाग, कूर्म, कृकल, और देवदत्त गौण प्राण या उपप्राण है। प्राण मात्र को मुख्य कार्य है। - आहार का यथावत परिपाक करना, शरीर में रसो को समभाव से विभक्त करना तथा वितरित करते हुए देहेन्द्रियों का तर्पण करना, जो कि देह के विभिन्न भागों में रक्त में आ मिलते हैं । देह के द्वारा भोगों का उपयोग करना भी इसका कार्य है।
3. मनोमय कोश- सूक्ष्म शरीर के इस पहले क्रिया प्रधान भाग को मनोमय कोश कहते है। मनोमय कोश के अन्तर्गत मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है जिन्हें अन्तःकरण चतुष्टय कहते है। पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं, जिनका सम्बन्ध बाहा्र जगत् के व्यवहार से अधिक रहता है।
4. विज्ञानमय कोश-सूक्ष्म षरीर का दूसरा भाग, जो ज्ञान प्रधान है, विज्ञानमय कोश कहलाता है। इसके मुख्यतत्व ज्ञानयुक्त वुद्धि एवं ज्ञानेन्द्रियां हैं। जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक विज्ञानमय कोश को ठीक से समझ कर उचित रूप से आचार-विचार करता है। और असत्य, भ्रम, मोह, आसिक्त आदि से सर्वथा अलग रह कर निरन्तर ध्यान व समाधि का अभ्यास करता है। उसे ऋतम्भरा प्रज्ञा उपलब्ध हो जाती है।

5. आनन्दमय कोश- इस कोश को हिरण्यमय कोश, ह्रदयगुहा, ह्रदयकाश, कारणशरीर, लिंगशरीर, आदि नामों से भी जाना जाता है। यह हमारे ह्रदय प्रवेश में स्थित होता है। हमारे आन्तरिक जगत से इसका सम्बंध अधिक रहता है, ब्राहा जगत् से बहुत कम। हमारा जीवन, हमारे स्थूल शरीर का अस्तित्व और संसार के समस्त व्यवहार इसी कोश पर अधिक है। निर्वीज समाधि की प्राप्ति होने पर साधक आनन्दमय कोश में जीवन मुक्त होकर सदा आनन्दमय रहता है।
ईश्वर क्या है? प्राण साधना


प्राण का मुख्य भाग नासिका है। नासिका छिदों के द्वारा आता जाता श्वास -प्रश्वास जीवन तथा प्राणायामका आधार है। श्वास -प्रश्वास रूपी रज्जु का आश्रय लेकर यह मन देहगत आन्तरिक जगत में प्रविष्ट होकर साधक को वहां की दिव्यता का अनुभव करा दे, इसी उद्देशय को लेकर प्राणायाम विधि का आविशकार ऋषि मुनियों ने किया था।
योग दर्षन के अनुसार- प्राणायाम अर्थात आसन की सिद्धि होने पर श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। हो वायु ष्वास लेने पर वाहर से षरीर के अन्दर फेफड़ों में पहुँचती है, उसे श्वास और श्वास बाहर छोड़ने पर जो वायु भीतर से बाहर आ जाती है, उसे प्रश्वास कहते हैं। प्राणायामक रने के लिए ष्वास अन्दर लेना ‘पूरक’, श्वास को अन्दर रखने को ‘कुम्भक’, रोचक ब्राह्राकुम्भक क्रियाएँ की जाती हैं। अच्छी तरह प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर नियमित रूप से विधिपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर जब नियमित रूप से विधिपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, तब के अनुसार ज्ञानरूपी प्रकाष को ढकने वाला अज्ञान का आवरण हट जाता है। और प्राणायाम सिद्ध होजाने पर मन में योग के छठे अंग धारणा की योग्यता आजाती है । जब श्वास शरीर में आता है तो मात्र वायु या आॅक्सीजन ही नहीं आती है। अपितु एक अखण्ड दिव्य शक्ति भी अन्दर आती है, जो शरीर में जीवन शक्ति को बनाऐ रखती है। प्राणायाम करना केवल श्वास का लेना और छोड़ना मात्र नहीं होता बल्कि वायू के साथ ही प्राण-शक्ति या जीवनी-शक्ति को भी लेना होता है। यह जीवन शक्ति सर्वत्र व्याप्त, सदा विद्यमान रहती है, जिसे हम ईश्वर, गाॅड या खुदा आदि जो भी नाम दें यह परम शक्ति तो एक ही है और उससे ठीक से जुड़ना और जुड़ रहने का अभ्यास करना ही प्राणायाम है।
प्राणायाम के लाभों को जानोगे तो पेरों के नीचे से जमीन खिसक जाऐगी
प्राण का आयाम (नियन्त्रण) की प्राणायाम ै। हमारे शरीर में जितनी भी चेश्टाऐं होती हैं, सभी का प्राण से प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध है। प्रतिक्षण जीवन और मृत्यु को जो अटूट सम्बन्ध मनुष्य के साथ है, वे भी प्राण के संयोग स ही है। प्राणायाम करने से मन के ऊपर आया असत, अविधा व क्लेश रूपी तम्स का आवरण क्षीण हो जाता है। परिशुद्ध हुए मन में धारणा, एकाग्रता स्वतः होने लगती है तथा धारणा से योग की उन्नत स्थितियों ध्यान एवं समाधि की और आगे बढ़ा जाता है।

योगासनों में हम स्थूल शरीर की विकृतिों को दूर करते हैं। सूक्ष्म शरीर पर योगासन की अपेक्षा प्राणायाम का विशेष प्रभाव होता है। सूक्ष्म शरीर ही नहीं प्राणायाम से स्थूल शरीर पर भी विशेष प्रभाव प्रत्येक्ष रूप से होता है।
यह जानकर आष्चर्य होगा परन्तु यह सत्य है की प्राणायाम से ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष सम्भव है।
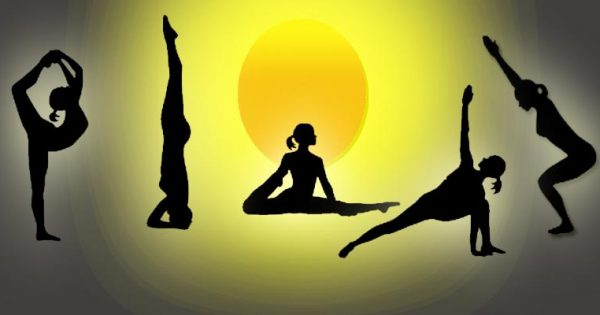
इन नियमों के आधार पर होता है प्राणायाम
1. प्राणायाम शुद्ध सात्विक निर्मण स्थल पर करना चाहिए। यदि स्म्भव हो तो जल के समीप अभ्यास करें
2. शहरों में जहां प्रदूशण का अधिक प्रभाव होता है। वहां प्राणायाम पहले ही घृत व गुगल से उस स्थान को सुगन्धित करें। अधिक नहंीं कर सकते तो घी का दीपक जलाइए।

3. प्राणायाम के लिए सिद्दासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठना उपयुक्त है। बैठने के लिए जिस आसन का प्रयोग करें वह विधुत कुचालक होना चाहिए
4. श्वास सदा नासिका से ही लेनी चाहिए। इससे विजातिय तत्व नास छिद्रों में ही रूक जाते हैं
5. योगासन की तरह प्राणायाम करने लिए भी कम से कम पांॅच घण्टे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। प्रातःकाल शोंच आदि से निवृत्त होकर योगासन से पूर्व प्राणायाम करें तो सर्वोत्तम है। शुरू में 5.10 मिनट अभ्यास करें तथा धीरे-धीरे बढ़ाते हुऐ आधा से एक घण्टा करना चाहिए। हमेशा नियत संख्या में करें। कम या ज्यादा न करें।

6. प्राणायाम करते समय मन शात एवं प्रसन्न होना चाहिए।
7. प्राणायामों को अपनी-अपनी प्रकृति और ऋतु के अनुसार करना चाहिए। कुछ प्राणायामों से शरीर में गर्मी बढ़ती हैं तो कुछ से ठण्डक व कुछ सामान्य होते हैं।

8. गर्भवती महिला, भूख से पीड़ीत, ज्वररोगी को प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
9. प्राणायामक दीर्ध अभ्यास के लिए पूर्ण ब्रहम्चर्य का पालन करें। भोजन सात्विक व चिकनाई मुक्त होना चाहिए।

10. प्राणायाम में श्वास को हठपूर्वक नहीं रोकना चाहिए।
12. प्राणायाम से पूर्व कई बार ‘ओउम’ का उच्चारण करना लाभप्रद है।
अगर इसको समझे तो हो जाआगें हमेश के लिए रोग मुक्त - प्राणायाम में उपयोगी बन्धत्रय
योगासान, प्राणायाम एवं बन्धों के द्वारा हमारे शरीर में जिस शक्ति का बहिगर्मन होता है, उसे रोखकर अन्र्तमुखी करते हैं बन्ध का अर्थ ही हैं बांधना या रोकना। ये बन्ध प्राणायाम में अत्यन्न सहायक है। बिना बन्ध के प्राणायाम अधुरे हैं।
1. जालन्धर बन्धः-
पद्मासन या सिद्धासन में सीधे बैठकर ष्वास को अन्दर भर लीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर टिके हुए हों अब ठोड़ी को थोड़ा नीचे झुकाते हुए कंठकूप में लगाना जालन्धर बन्ह कहलाता है। दृश्टि भूमध्य में स्थित किजिए। छाती आगे की और तनी हुई होगी। यह बन्ध कंठस्थान के नाड़ी जाल के समूह को बांधे रखता है।
लाभ- 1. कण्ठ मधुर, सुरीला और आकर्शक होता है।
2. कंण्ठ के संकोच द्वार इड़ा, पिंगला नाड़ियांे के बन्द होने पर प्राण का सुशुम्णा में प्रवेश होता है।

3.गले के सभी रोगों में लाभप्रद हैं, थायराइड, टांसिल आदि रोगों में अभ्यसनीय है।
4.विशुद्धि चक्र की जागृति करता है।
2.उड्डीयान बन्धः-
जिस क्रिया से प्राण उठकर, उत्थान होकर सुशुम्णा में प्रवेष हो जाए, उसे उड्डीयान बन्ध कहते हैं। खड़ होकर दोनों हाथों को सहजभाव से दोनों घुटनों पर रखिए। ष्वास बाहर निकालकर पेट को ढीला छोड़िए। जालन्धर बन्ध लगाते हुये, छाती को थोड़ा ऊपर की ओर उठाइए । पेट को अन्दर की तरफ करें । यथाषक्ति करने के पश्चात् पुनः ष्वास लेकर पूर्वदत्त दोहराइए। प्रारम्भ में तीन बार करना पर्याप्त है। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार पद्मासन या सिद्धासन में भी इस बन्ध को लगाना चाहिए।
लाभ- 1. पेट सम्बन्धी सम्स्त रोगों को दूर करता है।
2. प्राणों को जागृृत कर मणिपूर चक्र का षोधन करता है।

मूलबन्ध
सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर बाह्रा या आभ्यन्तर कुम्भक करते हुए, गुदाभाग एवं मूत्रेन्द्रिय को ऊपर की और आकर्शित करेें। इस बन्ध में नाभि के नीचे वाला हिस्सा खिच जाऐगा। यह बन्ध ब्राहाकुम्भक के साथ लगाने में सुविधा रहती है। वैसे योगाभ्यासी साधक इसे कई-कई घण्टों तक सहजावस्था में भी लगाये रखते हैं।
लाभ- 1. इससे अपान वायु का ऊध्र्व-गमन होकर प्राण के साथ एकता होती है। इस प्रकार यह बन्ध मुलाधार चक्र की जागृती करता है।
2.कोश्ठबद्धता और बवासीर को दूर करने तथा जठराग्नि को तेज करने के लिये यह बन्ध अति उत्तम है।
3.वीर्य को ऊध्र्वरेतस् बनाता है। अतः ब्रहा्रचर्य के लिए यह बन्ध महत्त्वपूर्ण है।
महाबन्ध
पद्मासन आदि किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठकर तीनों बन्धों को एक साथ लगाना महाबन्ध कहलाता है । इससे वे सभी लाभ मिल जाते हैं, जो पूर्व निर्दिश्ट हैं
लाभ- यह बन्ध महाबलषाली बनाता है।


Comments
Post a Comment